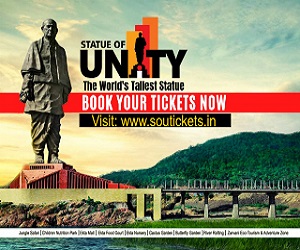अनकही-अनसुनीः नवाबी शहर लखनऊ की नज़ाकत और नफासत की कहानी
- Sonu
- Saturday | 15th July, 2017
- local

- तहज़ीब कोई मेरी आँखों में जंचेगी क्या
- मेरी निगाह ए शौक़ ने देखा है लखनऊ
- कभी पाक के लोग भी थे लखनवी ज़ुबान के दीवाने
By: अश्विनी भटनागर
लखनऊः कुछ साल पहले, मैं और मेरी पत्नी पेरिस एयरपोर्ट की लाउन्ज में बैठे बातचीत में मशगूल थे कि अचानक पीछे की सीट से आवाज़ आयी, माफ़ किजयेगा मैं आप लोगों की गुफ़्तुगू सुन रहा था और अपने को रोक नहीं पाया, क्या आप लखनऊ से है?
आप ऐसा क्यों पूछ रहे है, मैंने कहा। हम तो रोज़मर्रा की जुबान बोल रहे है। उस शख्स ने हंस कर कहा, जी, उर्दू तो हम भी बोल लेते है पर लखनवी ज़ुबान का लहजा ही कुछ और है। जल्दी पहचान में आ जाता है।
वो शख्स लाहौर का रहने वाला था पर उसके खानदान का एक हिस्सा लखनऊ से तालुक रखता था। जब भी खाला जान गर्मी की छुटियों में हमारे पास आती थी तो घर में उनकी ही ज़ुबान गूंजती थी। हमारी मां हम सब से कहा करती थी अब भी वक़्त है शोहदों आवारापन छोड़ दो और कुछ नफासत लियाक़त सीख लो लखनऊ वालों से। पता नहीं फिर मौका मिले या न मिले।
ऐसा ही वाकया हमारे साथ सैन फ्रांसिस्को में भी हुआ। एक जगह हम लोग कबूतरों को दाना खिला रहे थे और हंस-बोल रहे थे कि अचानक किसी ने हमे टोका। लखनऊ से तशरीफ़ लाये है हुज़ूर?
वह शख्स भी लखनऊ का नहीं था पर लखनवी लहजे से उसका तालुक पुराना था। वो हमे सीधे ले गए 1960 के चारबाग़ रेलवे स्टेशन पर जहां तांगेवाले से लेकर रिक्शावाले भी लियाक़त की मिसाल हुआ करते थे। हम लोग रहने वाले तो जौनपुर के है पर मैंने दो साल लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। फिर मैं अमेरिका ऐसा आया कि वापस जाना ही नहीं हुआ। तीस पैतीस साल हो गए है पर लखनवी खनक कांनों से जाती ही नहीं।
असल में 18वीं शताब्दी के शुरुवाती सालों में शुरू हुई लखनवी नफासत, नज़ाकत और तहजीब अपने पूरे शबाब पर 1857 तक पहुंच गयी थी। लखनऊ के नवाबों की आन, बान और शान दिल्ली के दरबार से कई गुना ज़्यादा थी। ग़ालिब और मीर जैसे शायर मुग़लिया दरबार को छोड़ लखनऊ का रुख कर चुके थे। कैसरबाग, हज़रतगंज, अमीनाबाद, चाइना बाजार वगैराह चांदनी चौक पर भारी पड़ने लगे थे। लखनऊ का चौक इलाका तो पहले से ही खुशगवार था।
1857 का गद्दर और उसमें हार के बाद, लखनऊ के नवाबों की गद्दी तो छीन गयी पर उन की तहज़ीब कायम रही। मख़मली चुन्नट पड़े कुर्ते, बेहतरीन अचकने, रूमाली टोपियां, घाघरे और सरारे, लजीज़ खाने और जन्नत बक्श तावाइफे लखनऊ के मिजाज को अपनी पहचान देती रही।
ये सिलसिला 1960 तक बखूबी चला। उस वक़्त शायद ही ऐसा कोई लखनवी जिसकी ज़ुबान से ऐहमक से ज्यादा बड़ा शब्द कभी फिसला हो। असल में सिर्फ इतना कह देना कि फलां का जिक्र जुबान पर न लाये काफी होता था। किसी की शान की बकिया उधेड़ना तहज़ीब दारों को सख्त नापसंद था चाहे वो शख्स जानी दुश्मन ही क्यों न हो।
साठ के अंत होने तक हिंदी आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। ऐहमक कहना कम हो गया। लुर्र ने उसकी जगह ले ली। उसके साथ जुड़ गए आसपास से लाये हुए नए शब्द जैसे मग्गाह, घामड़, चिरकुट, लल्लू वगैराह।
अब झापड़ रसीद नहीं किये जाते थे बल्कि लोग कंटाप मारने लगे। ईंट से ईंट बजाने की हरकत से भी लोग बाज आने लगे और उसकी जगह गुम्मा ले कर लोगों को हड़काने लगे। आप-जनाब धीरे-धीरे अबे-तबे में तब्दील होने लगा था। लखनऊ ढ़हने लगा था।
मंगल के दिन हज़रतगंज के हनुमान मंदिर पर भीड़ लगती थी। भक्त प्रसाद चढ़ाते थे तो और लोग हल्का सा सर झुकाते हुए मंदिर के सामने से गुज़र जाते थे। चैराहे पे रोवर्स खुल चुका था और 1970 में वहां कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा सॉफ्टी भी मिलने लगी थी। बीटल्स के अंग्रेजी गाने भी लखनऊ पहुंच चुके थे। लड़कों का झुंड जब मंदिर के सामने से निकलता तो बड़ी श्रद्धा से हाई-हनु कहता हुआ जाता था।
हाई और बाय के चलन के साथ-साथ, लखनऊ चिड़िया का है या फिर भूतनी का जैसे प्रिय वाचक शब्दों से भी हिलमिल गया। यूनिवर्सिटी में नारों में टेम्पो हाई है का इस्तिमाल होने लगा, लोग लल्लन टॉप हो गए और नफासत, नज़ाक़त के चलते हमारा वजूद खत्म होता गया।
1857 से 1947 तक जो अंग्रेज नहीं कर पाए उसको हमने सिर्फ 1970 के दस सालों में कर लिया। यानी लखनवी तहबीज को एक छोटे से वक़्त में नेस्तो नाबूत कर दिया। शायद यह दशक लखनऊ के इतिहास में वो ही महत्व रखता है जो कि 1857 के बाद के साल रखते थे। अंग्रेज़ों ने तो इमारते गिरा कर सिर्फ शहर की शक्ल ही बदली थी। हमने तो उसकी रूह भी कुचल दी है।